साइबेरिया का सफ़ेद सारस
जहांगीर के जमाने में एक नामी चितेरा हुआ था- उस्ताद मंसूर नक़्क़ाश। मुग़लिया मुसव्विरों में उसकी जोड़ का कोई आदमी न था। नादिर-उल-अस्र। (अपने) समय में सर्वश्रेष्ठ। जीव-जिनावर जस के तस कागज़ पर कोर देता था। उतने ही सुंदर बेल बूटे भी। उसने कश्मीर के लाला फूलों के चित्र बनाए और कोरा हब्शियों के देश का धारीदार ज़ेबरा, और अमेरिकी मुर्ग़, और डोडो कबूतर। और उसने उकेरा एक अकेला सारस। पर यह सारस सलेटी रंग का, लाल छपके वाला सदा का सा सारस न था। यह रंग से धौला झक्क था। जिसकी आंखों की कोरें ज़र्द और पाँखों की कोरें कुहली।
यह अनोखा सारस उसे मिला कहाँ होगा? क्या यह बादशाह का पालतू था, लैला मजनूं कहे जाने वाले सारस के उस जोड़े के जैसे ? या मंसूर को यह दिखा होगा किसी पोखर में? या कि आगरे के चिड़ीमार टोले वालों में से कोई इसे उठा लाया था तस्वीरखाने तक, ताकि मंसूर उसे कागद में कैद कर सके ? इन बातों की तफ़्सील हमें नहीं मिलती। तस्वीर पर जहाँगीरी मुहर लगी है और हाशिए पर केवल इतना लिखा है- अमल-ए- उस्ताद मंसूर। इसके सिवा आगा-पीछा कुछ नहीं।
मंसूर से कोई डेढ़ सौ बरस बाद पश्चिम के खग-विज्ञानियों को पहली बार इस पक्षी की पहचान हुई। ओब-इरतिश नदियों के किनारे, याकूतों की सरजमीं साइबेरिया में। तब मालूम हुआ कि यह सफ़ेद सारस वहीं का रहवासी है। भारत में तो यह बस जाड़ा काटने उतरा करता है।
मंसूर ने यह सारस कहाँ देखा था, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन ह्यूम ने इसे लेह-लद्दाख से लेकर इटावे-मैनपुरी तक छितरे हुए पाया था। ह्यूम याने एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। अब उनकी पहचान भले भारत की कॉंग्रेस खड़ी करने वाले होने तक सिमट कर रह गई हो, पर अपने जमाने के वे आला दर्जे के ओरनिथोलॉजिस्ट थे। खग-विज्ञानी।
ह्यूम ने जब पहली बार यह सफेद सारस देखा, तो पहला काम उन्होंने गोली चलाने का किया। इसकी देही का नमूना रखने के लिए। पर बाद में कहते पाए गए कि ओरनिथोलॉजी में सबसे बुरा काम यही है। साइन्स के नाम पर शिकार! ख़ैर, क्रौंच वध तो कईयों में करुण रस जगा चुका।
यों ह्यूम साहब के मामले में एक बार इससे हास्य रस भी जगा। हुआ यूं कि साहब भैंस की ओट लेकर पोखर में इस परिंदे का शिकार खेलने गए थे। अब एक तो उसके भाव पहले से ही 'लटक मत पटक दूंगी' वाले थे; दूसरा, ह्यूम साहब ही के शब्दों में- भैंस गोरों पर भला कब भरोसा करती है ? ज्यों ही बन्दूक छूटी, भैंस चमक कर तुड़ा भागी। गए ह्यूम साहब पानी में! चाम पर मार्के तो बने ही, बारूद की कुप्पी गुमी सो अलग। फिर साहब कभी पोखर में नहीं उतरे।
ह्यूम मानते थे कि ऐसी कोई तस्वीर बनी ही नहीं, जो इस सारस की सुघड़ता के साथ न्याव कर सके। बात ठीक ही थी। पाँखों का एक जोड़ा काळा, बाकी पूरी काठी उजल कपासी। रूई के फाहे जैसा गात। सुराही-दार गर्दन, जिस पर लोहू रंग की लंबोतरी चोंच चेपी हुई। आंखें ज्यों दो पीली घुंडियां। पियाज़ी रंग के पैर। कद ऐसा कि मिनख के माथे तक नहीं तो खवे तक तो आ ही जाए। दो-दो हाथ लम्बे डैने। कुल मिलाकर दिखने में एकदम शाहाना। जिसके ठाट ठहर कर देखे जाएं। जिसे देखने को मज्मे और मेले लगें। ऐसी कुदरत को किसकी कूची मात देगी भला।
आज भारत में बहुत कम लोग हैं, जो इस इम्तियाज़ी सारस को चीन्हते हैं। इसे देख चुके तो इने गिने। ऐसा इसलिए कि कोई बीस बरस हुए, अब इसकी रम्मत यहाँ से उठ चुकी है। मैं भी कागद की लेखी ही कहता हूँ, मेरी आँखन की देखी यह शै नहीं। कागद ये कहते हैं कि भारत में यह सफ़ेद सारस आख़िरी बार 2002 में देखा गया था। घना, भरतपुर, राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क। यहां हर बरस यह बर्फ़ का फूल खिला करता था। साल में चार महीने। कातिक,अगहन,पूस और माघ।
दरअसल, साइबेरियाई सफ़ेद सारस की आबादी तीन टुकड़ों में बंटी हुई थी: पूर्वी, पश्चिमी और दरमियानी। इनमें से दरमियानी दल साइबेरिया में कुनोवात नदी के किनारे से उठता, फिर कज़ाखों, उज़्बेकों के मुल्कों से होता हुआ नीचे उतरता। अफ़ग़ानिस्तान के आब-ए-इस्तादा में कुछ रोज़ यह ठहरा करता था। तब यह भरतपुर पहुंचता, जहां इसके भाई बन्धुओं की भीड़। हवासिल, कुरजां, अंजन, सुरमई, जांघिल और घोंघिल। और भी पचासों प्रजातियाँ। परदेसी परिंदों का पैराडाइज। सफ़ेद सारस का तो पिछली एक सदी से भारत में इकलौता ठौर था घना।
अब ऐसी जगह से भी इसकी रम्मत भला क्योंकर उठ गई? इसलिए कि घना के दुःख भी घनेरे। दरअसल, केवलादेव कुदरती झील नहीं है। यह मानव निर्मित मुर्गावी शिकारगाह है। जो भरतपुर के महाराजा रामसिंह और किशनसिंह के समय में बन कर तैयार हुआ। मोरबी के कुंवर हरभाम की दीवानी के दौरान। अंगरेज़ी तर्ज़ पर ही बना था, सो अंग्रेज़ो के मनभावन। बरतानिया हुकूमत के आला अफ़सर यहां बत्तखें मारने आया करते थे। राजे-रजवाड़े भी। एक-एक दिन में हजारों-हजार पखेरू मारे जाते। घना में लगे एक 'टैली बोर्ड' पर अभी भी इन सब का हिसाब लिखा है। वायसराय लिनलिथगो की विजिट का गेम इस टैली का टॉपर। 39 बन्दूकों से 4,273 के स्कोर के साथ। अब इन में सफ़ेद सारस कितने, किसको मालूम ? जब बोरे भरे जा रहे हों, तब यह कौन गिने कि कितनी कैमा, कितनी शामा, कितनी कुरजां, कितनी फिरोजा।
एक समय में भरतपुर की प्रजा भी घना की घनघोर विरोधी हुआ करती थी। अव्वल तो इसका इतराज था बेगार को लेकर। जब भी घना में बत्तखें मारी जातीं, तो बहुत से काम बेगार में करवाए जाते थे। जैसे- ज़ख़्मी बत्तखें तुरन्त पकड़ कर मारना, मरी हुई बत्तखें जमा कर के बोरे में भरना, आस पास के गांवों में पोखरों से चिड़ियों को उड़ाना आदि। और यह सब कुछ करना भी थोड़े से गुड़ और भुने हुए चनों की एवज में। परिणामतः प्रजामण्डल के समय में इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन हुए।
दूजे, आज़ादी के बाद भी महाराजा ने यहां पर अपने 'शूटिंग राइट्स' बरकरार रख लिए थे, जिससे लोग खार खाए हुए थे। 'उठो किसानो, कर लो चेत; काटो रुन्ध, बनाओ खेत' क्रांति गीत बन गया। किसान क़ौमें घना पर हल चला देने को मंड आई। तब नेहरू के हस्तक्षेप से इसे अभयारण्य का दर्ज़ा मिला।
तीसरे, नेशनल पार्क बनने तक गिर्द के गांवों के ढोर डंगर घना में ही चरा करते थे। चराई पर रोक लगी, तो लोग लड़ भिड़े। घना में फिर से बन्दूकें बोलीं। अघापुर के सात लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। आगे अजान बांध के पानी को लेकर लड़ाइयाँ हुईं। कई बार परिंदों के हिस्से का पानी रोक दिया गया। कई बार कुदरती काळ पड़ गए। कई दावानल भी केवलादेव ने देखे। इसी कर तो मैंने कहा घना के दुःख घनेरे।
घना बना रहा, क्योंकि घना के संकटमोचक थे- डॉ. सलीम अली। विख्यात खग विज्ञानी। बर्डमैन ऑफ इंडिया। इनके प्रभाव में नेहरू और इंदिरा, पिता-पुत्री दोनों ही थे। 'डॉक्टर साहब' ने घना के लिए अपने इस असर का इस्तेमाल बहुत बार किया। पक्षी विहार बनवाने में, महाराजा के शूटिंग राइट्स रद्द करवाने में और नेशनल पार्क घोषित करवाने में सलीम अली का ही हाथ था।
प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी जब परिवार के साथ भरतपुर भ्रमण पर थीं, तब सलीम साहब ने उन्हें वह प्रियदर्शन पक्षी दिखलाया- सफ़ेद सारस। साथ ही वे कारण भी बतलाए, जिनके कारण इसकी संख्या कम होती जा रही थी। सफ़ेद सारस, जो ह्यूम के समय हज़ारों की तादाद में हुआ करते थे,सलीम के समय सौ से भी कम रह गए थे।
इंदिरा उन दिनों दुनिया भर के ऐसे साइंसदानों से जुड़ी हुई थीं, जो कुदरत के लिए काम किया करते थे। इनमें अमेरिका के जॉर्ज आर्चीबाल्ड भी थे, जो इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन चलाया करते हैं। उन्होंने जब केवलादेव में 'साइब्स' के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की तो इंदिरा ने इसे हाथों हाथ लिया। इन्हीं की सलाह पर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के हुक्मरानों को चिट्ठियां भी लिखीं। ताकि सफ़ेद सारस का रास्ते में होने वाला शिकार रोका जा सके। इंदिरा ने इस पर डाक टिकट भी जारी करवाया। अपने पर्सनल कलेक्शन से तैलचित्र उधार दे कर। जो कि डायेन पियर्स का कोरा हुआ। पर इस क्रौंच के भाग में कोरी तस्वीरें, और कुछ नहीं। गिरती गिनती नहीं रुकी।
आगे घना कई बरसों तक इस मेहमान की मान मनौव्वल करता रहा। यहाँ उगने वाले मोथिये की जड़ें इस परिंदे की पसन्दीदा ख़ुराक थी। उन्यासी में जब केवलादेव में काळ पड़ा, तो पाताल तोड़ कुएं खुदवाए गए। पर आग लगने के बाद! कुएं इतने देरी से खुदे कि उस साल मेहमान आया तब तक मोथिया उगा ही नहीं। और अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। मनुहारों का मतलब नहीं रहा। इन दो बरसों में भारत आने वाले दरमियानी दल की आबादी लगभग आधी हो चुकी थी।
उधर, पूरबी दल में अभी भी हज़ारों साइब शामिल थे, जो जाड़े में चीन की पोयांग झील पहुंचा करते थे। चूंकि कुनोवात के वाइल्ड साइब्स में अंडे देने वाले कोई जोड़े बचे न थे, सो जॉर्ज याकूतिया से इन पुरबियों के अंडे उठा लाने लगे। आईसीएफ के अमेरिकी और सोवियत सेंटर पर इन्हें सेया जा कर चूजे पाले गए। बड़े होने पर इन्हें कुनोवात के किनारे छोड़ दिया जाने लगा, इस उम्मीद के साथ कि वे झुंड के साथ उड़ेंगे तो दरमियानी दल के माइग्रेशन का मार्ग जान लेंगे। पर अफ़सोस कि ऐसा हुआ नहीं। पाले गए पखेरू या तो उड़े नहीं, जो उड़ गए वे पहुंचे नहीं।
जॉर्ज ने यहाँ केवलादेव में भी अपने पाले कुछ साइब्स ला कर छोड़े। पहले-पहल बिगुल नाम का एक परिंदा। फिर 'व्हाइट'। उसके बाद बिली, बुशी,बोरिस,गोरबी। फिर अल्कोनोस्त, अनबुर, अरफ़ात और बहरामी...। इन सब का भी वही हश्र हुआ जो कुनोवात वालों का हुआ था।
साइब अपने लेखे में उमर बड़ी लम्बी लिखवाकर लाते हैं। साठ-सत्तर-अस्सी साल का जीवन। सो, जो जीवित थे, वे बरसान बरस मुड़-मुड़ घना आते रहे। पर यहां लोग उंगलियों पर गिनते, तो हर बार एक दो पोर छोड़ने पड़ते। आखिर में एक बरस पांच परिंदे पहुंचे, एक बरस तीन। 2001 की सर्दियों में दो साइब इधर आए थे, उन्होंने 2002 के लगते फागुन उड़ान भरी। फिर पलट कर नहीं लौटे। रम्मत पूरी हुई। अध्याय समाप्त। दरमियानी दल की आबादी का अवसान।
साइब्स का पश्चिमी झुंड जो ईरान में उतरा करता था, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। यहां ये माज़ंदरान में जाड़ा काटते थे। इधर आने वाले आख़िरी जोड़े को ईरानियों ने नाम दिया था : ओमिद और आरेज़ू। आरेज़ू 2008 में खेत रही। ओमिद अकेला रह गया। अगले पन्द्रह बरस तक वह अकेले ही माज़न्दरान आता रहा। ईरानी हर बरस इंतज़ार करते रहे। ओमिद का आना त्योहार तक बन गया था। जॉर्ज ने भी यहां 'रोयां' नाम की पालतू साइब को ओमिद के साथ किया, ताकि वह माइग्रेशन का मार्ग सीख सके। पर उससे भी पार नहीं पड़ी। पिछले साल, 2024 में, ओमिद लौट कर नहीं आया। इस झुंड की आख़िरी 'ओमिद' भी मिट गई।
चीन चूंकि पहले चेत गया था, सो पोयांग में अब भी पूरबिये उतरा करते हैं। वहां रम्मत जमी हुई है। लगभग चार हज़ार खेलारों के साथ। इधर, भरतपुर इन बीस बरसों में इस मेहमान को भूल बैठा है। घना में दूरबीन टांगे घूमते कुछ लोगों के सिवा किसी को साइब याद नहीं।



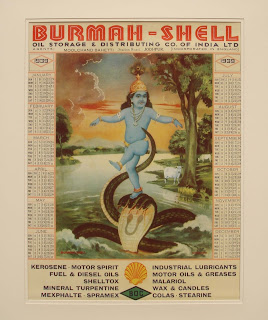
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें