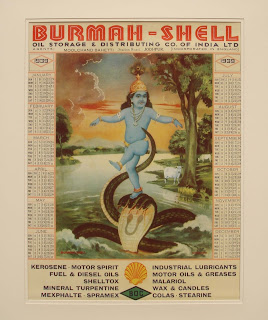नीलीसन्धान

ज़्यादा दिन नहीं बीते जब कि रंगतें चढ़ाने के सारे साधन कुदरती हुआ करते थे। फूल-पत्तियाँ, छाल और जड़ें तथा कुछेक खनिज। ज्यों आल की लकड़ी और मजीठे की जड़ों से लाल रंग निकाला जाता था। कसूमे के फूल से मिलता था जेठा, प्याजी और नारंजी। आम्बाहल्दी पीला रंग देती थी, खैर देता था कत्थई और बिदामी। इसी तरह नील के पौधे से निकलते थे आसमानी, फिरोज़ी और सुरमई रंग। पर नील एक मायने में इन सब से न्यारी थी। फरक ये था कि आम्बाहल्दी की तरह पानी में घोलने से कपड़े पर इसका रंग नहीं चढ़ता था; न ही यह आल-मजीठे, कत्थे और पतंगे की तरह फिटकड़ी की लाग से रंग देती थी। नील का रंग चढ़ाने का ढब निराला था। एकदम अलहदा। इतना अलग कि एक समय में नीला रँगने वालों की जात तक जुदी हो गई थी। बाकी सारे रंग चढ़ाने वाले रँगरेज, नीला रँगने वाले नीलगर। आज की कहानी नील के इसी काम की कहानी है। यह काम जुगत का जरूर था, किन्तु था बड़ा अरोचक। इसका नुस्खा कुछ यूँ था कि पहले नील के पौधे से नील-बट्टी बनाई जाती थी। इसके लिए अधपके पौधों को पानी में सड़ा-गला कर, खूंद-मसल कर नील का घोल तैयार किया जाता था। इस घोल को कड़ाहों में औटा कर गाढ़ा कर लेते थे।...